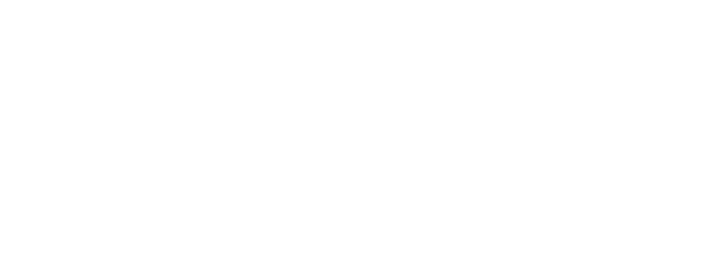Currently Empty: $0.00
सतत व्यवसायिक विकास
किसी भी व्यवसाय में प्रभावकारी कार्य कुशलता के साथ कार्य करने के लिए उसके अनुरूप विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि कार्य की आवश्यकता के अनुसार दक्षता, योग्यता और ज्ञान को अवश्य विकसित किया जाए जिससे व्यक्ति अपने कार्य को उतृष्ट तरीके से करने में सक्षम हो सके।
अतः सतत व्यवसायिक विकास नियमित रूप से ज्ञान, दक्षता और निपुणता विकसित करने की प्रक्रिया है तथा प्रभावशीलता के लिए इसे उसी स्तर पर बनाए रखने की आवश्यकता भी है। किसी व्यवसाय के लिए आवश्यक ज्ञान और दक्षता को औपचारिक तरीके से नियमित संचालित होने वाले पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर प्राप्त किया जा सकता है या अनौपचारिक रूप से कार्य के दायित्व का निर्वाह करते हुए अथवा परिचर्चा करके या अवलोकन करके प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति जो व्यवसायिक क्षेत्र में कार्य कर रहा है। उससे सीखने और सुधार करने के संकल्प की अपेक्षा अवश्य किया जाता है। सतत व्यवसायिक सुधार (सी०पी०डी०) एक-दूसरे से जुड़ी हुई अनेक प्रक्रियाओं का योग होता है। यह क्रिया-कलाप विकास की आवश्यकता का आंकलन करने से शुरू होती है। फिर अनेक प्रकार की सीखने की प्रक्रियाओं को चित्रित करना होता है। इसके लिए व्यक्ति को कार्य कुशलता के साथ कार्य करने के लिए कहा जाता है और दूसरों से उसे सांझा भी करना होता है। इस प्रकार व्यक्ति की कार्य कुशलता का एक प्रतिपुष्टि प्राप्त हो जाता है। जिसके आधार पर सीखने की प्रक्रियाओं में सुधार किया जाता है।
प्रत्येक व्यक्ति विलक्षण होता है और अपनी आवश्यकता पहचानने का उसका एक विशिष्ट तरीका होता है उसी तरह अपनी सुविधा के अनुसार सीखने की व्यवस्था करता है और अपने तरह से सीखना चाहता है।
सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि व्यवसायिक व्यक्ति अपने कार्य की जिम्मेदारी अवश्य उठाए और सुधार के लिए सीखने की आवश्यकता को अवश्य पहचाने|
व्यवसायिक विकास निम्न क्रम से मिलकर बना होता है-
1. आवश्यकता का आंकलन: सुधार के लिए आवश्यकता का आंकलन अति आवश्यक है, इस प्रक्रिया में वर्तमान और भविष्य के आवश्यक स्तर को पहचान कर इसके बीच के अन्तर को पता लगाया जाता है और इसे दूर करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। व्यवसायिक संस्थान विशेषज्ञों या संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दक्षता का आडिट कराया जाता है। शिक्षकों, प्रशिक्षकों तथा वरिष्ठों से प्रतिपुष्टि प्राप्त कर व्यवसायिक क्षमता की कमियों का पता लगाया जाता है। सशक्त और कमजोर क्षेत्र का पता लगाकर किसी विशेष क्षेत्र के विकास की आवश्यकताओं का पता लगाया जाता है। आवश्यकता की पहचान निम्न में से किसी भी कारक के लिए हो सकती है|
1. वातावरण सम्बन्धित: आत्यधिक आवाज ध्यान केंद्रीत करने में बाधक होता है। जिससे व्यक्ति अपना कार्य नहीं कर सकता है।
2. व्यवहार सम्बन्धित: व्यक्ति को सम्प्रेषण में ज्ञान की कमी के कारण बाधाएँ आती है।
3. क्षमता: व्यक्ति को कार्य करने का ज्ञान नहीं होता है।
4. विश्वास और मानवीय मूल्य: इसकी कमी कार्य करने में बाध उत्पन्न करते हैं।
5. पहचान: व्यक्ति किसी कार्य के करने के तरीके को नहीं जानता है।
जब विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्र को चित्रति कर लिया जाता है तब अगला कदम कार्य प्रक्रिया की उचित योजना होती है।
2. उचित योजना और प्रशिक्षण: विकास के लिए प्रशिक्षण कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में दिया जाता है यह प्रशिक्षण औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार का हो सकता है। औपचारिक तरीका किसी संस्थान द्वारा संचालित और मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम हो सकता है। यह पाठ्यक्रम कक्षा में हो सकता है या ऑन लाइन भी हो सकता है। अनौपचारिक प्रशिक्षण का तरीका, सलाह, सुझाव, पढ़ना और वीडियो प्रशिक्षण में से कुछ भी हो सकता है। इस प्रशिक्षण में कार्य करते-करते सीखने का अवसर होता है।
3. सीखने को लागू करना: व्यक्ति प्रशिक्षण में जो कुछ सीखा है, अब उसे कार्य परिवेश में लागू करना होता है क्योंकि सतत व्यवसायिक विकास का यह मुख्य अंग है। यह आवश्यक है कि प्रशिक्षण में प्राप्त सीख कक्षा तथा कार्य में दृष्टिगोचर होनी चाहिए, तभी व्यवसायिक विकास सम्भव हो सकता है। यह आवश्यक है कि परिवर्तित होने वाली प्रक्रियाओं का अभ्यास किया जाए इसके अन्तर्गत निम्नवत प्रक्रिया होती है-
1. पढ़ना: जो कुछ भी सीखा गया है उस विषय को विकास के लिए पढ़ना होता है।
2. पूछना: यह पूछना कि दूसरे शिक्षक किस प्रकार करते है और क्यों करते है।
3. अवलोकन करना: एक अनुभवी शिक्षक के कक्षा में उसकी अनुमति से उसके क्रिया-कलाप को देखना, अर्थात वह कैसे पढ़ाता है।
4. बात करना: संस्थान/संगठन में अन्य लोगों के साथ अपने विचार और अनुभव को सांझा करना।
5. अनुभूति करना: विकास के संदर्भ में अपने आवेश और अनुभूति का ध्यान रखना, नकारात्मक अनुभूतियों को दूर करने की कोशिश करना।
6. सोचना: स्वयं का मूल्यांकन करना और सीखना। अपने शिक्षण की प्रभावशीलता का पता लगाने के लिए समय निकालकर सोचने की कोशिश करना।
4. प्रतिपुष्टि और सुधार: विद्यार्थियों, वरिष्ठों व सहयोगियों से प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर शैली, सम्प्रेषण दक्षता, प्रश्न पूछने का तरीका, प्रस्तुतीकरण की योजना तथा सम्पूर्ण उपयोग की कार्यनीति में सुधार करना। यह व्यक्ति (शिक्षक) की योग्यता, क्षमता और प्रभावशीलता के सुधार में सहायता करता है, यह एक दिन या एक सप्ताह की प्रक्रिया नहीं है। धीरज के साथ सतत परिश्रम करने से ही सुधार सम्भव होता है और धीरे-धीरे व्यक्ति अपने व्यवसाय में पारंगतता प्राप्त कर लेता है।
5. अपने विचार और दृष्टिकोण को सांझा करना: अपने सीखने, पढ़ने तथा सुधार के तरीके का अपने मित्रों सह-शिक्षकों, विशेषज्ञों तथा शिक्षाविदों के साथ सांझा करना और उसमें परिचर्चा करना, हमेशा विकास का एक उत्तम तरीका होता है। अपने व्यवसाय में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए यह तरीका एक उत्तम उपकरण की तरह कार्य करता है जिससे व्यवहार को प्रश्चित करना सरल हो जाता है। यह व्यक्तिगत और व्यवसायिक विकास के लिए नए विचारों का सृजन भी करता है|